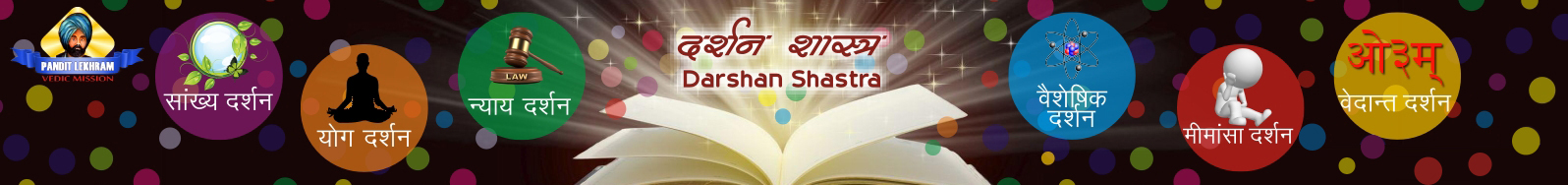सूत्र :दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्णा वैराग्यम् ॥॥1/15
सूत्र संख्या :15
व्याख्याकार : स्वामी दर्शनानन्द
अर्थ : पद०- दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य । वशीकारसंज्ञावैराग्यम् ।
पदा०- (दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य) इस लोक तथा परलोक के विषयों की तृष्णा से रहित पुरूष के चित्त की स्थिति को (वशीकारसंज्ञावैराग्यम्) वशीकार नामक अपन वैराग्य कहते हैं।।
व्याख्या :
भाष्य- स्त्री, पुत्र, ऐश्वर्य आदि चेतन, अचेतन इस लोक में होने वाले विषयों को “दृष्टविषय” और परलो से लेकर प्रकृतिलय पर्य्यन्त विषयों को “अनुश्रविक” विषय कहते है, गुरूकृत उच्चारण के अनन्तर सुने जाने से वेद का नाम “अनुश्रव” और वेद से जो विषय जाने जायं उनका नाम “अनुश्रविक” है।।
वेद में परलोक तथा प्रकृतिलय आदि विषयों का वर्णन इस प्रकार आया है कि:-
द्वेस्त्रुतीअश्रृणवंपितृणामहं देवानामुतमत्र्यानाम्।
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेतियदन्तरापितरं मातरं च।। ऋ० ८१४११२
अर्थ - कर्मों, विद्वानों और साधारण मनुष्यों के लोक परलोक में जाने के लिये जन्म मरण रूपी दो मार्ग हैं, इन्हीं दो मार्गों से सम्पूर्ण जीव इस लोक से परलोक में और परलोक से इस लोक में जाते और आते हैं, इन दो मार्गों की प्राप्ति का कारण माता और पिता हैं, यहां लोक से तात्पर्य इस जन्म का और परलोक से जन्मान्तकर का है।।
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते।
ततोभूय इ वते तमो य उ सम्भूत्याँरता: ।। यजु०४०। ९
अर्थ- जो पुरूष असम्भूति=प्रकृति की ईश्वर मानकर उपासना करते हैं वह अन्धतम=गाढ़ अन्धकार को प्राप्त होते हैं और जो सम्भूति=प्रकृति के काय्र्यों की ईश्वरभाव से उपासना करते हैं वह और भी अन्धतम को प्राप्त होते हैं।।
असंभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयँसह ।
विनाशेन मृत्युंतीत्र्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते।। यजु० ४० । ११
अर्थ- प्रकृति की ईश्वरभाव से उपासना करने वाले अमृत=चिकाल तक अमरणरूप प्रकृतिलयता को प्राप्त होते हैं अर्थात् चिरकाल तक प्रकृति में लीन होकर रहते है, प्रकृति में लीन होने का नाम ही अन्धत है और प्राकृत पदार्थों की ईश्वरभाव से उपासना करने वाले कुछ काल तक मृत्यु अतिकमण करजाते अर्थात् स्थूलशरीर से रहित होकर उन्हीं प्राकृत पदार्थों में लीन पुरूषों का नाम विदेह है, इनका वर्णन १९ वें सूत्र में विस्तार पूर्वक करेंगे।।
इन दोनों प्रकार के विषयों में दुःखरूपता का अनुसन्धान करने से जिस पुरूष की इच्छा निवृत्त होगई है वही योग का अधिकारी है, उस योग के अधिकारी की जो लोक तथा परलोक के विषयों में हेय उपादेयभाव से रहित चित्तस्थिति अर्थात् उपेक्षा बुद्धि है उसी का नाम अपरवैराग्य है।।
इस वैराग्य के यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार यह चार भेद हैं, इन सबका यथाक्रंम पृथक २ लक्षण करना उचित था परन्तु प्रथम के तीन वैराग्यों का आचार्य्य ने इसलिये पृथक् २ लक्षण नहीं किया कि उनकी प्राप्ति के बिना चैथे की प्राप्ति नहीं होसकती अर्थात् तीनों की सिद्धि के अनन्तर ही वशीकार वैराग्य की प्राप्ति होती है, इन चारों वैराग्यों के लक्षण इसप्रकार हैं कि चित्त में जो राग द्वेष आदि दोषरूप मल हैं उन्हीं के कारण इन्द्रियों की अपने २ विषयों में प्रवृत्ति होती है “मेरे इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति न हो” ऐसा विचारक मैत्री आदि भावना के अनुष्ठान को “यतमानवैराग्य” कहते हैं, यतमान के अनन्तर ऐसा विचार करना कि मेरे चित्त के कई द्वोष निवृत्त होगये हैं और कई निवृत्त हो रहे हैं अथवा इसी प्रकार शेष भी निवृत्त होजायेंगे, इस प्रकार निवृत्त हुए दोषों के निर्धारण को “व्यतिरेकवैराग्य” कहते हैं, जब चित्त के मल निवृत्त होजायँ तब विषयों में प्रवत्ति के लिये सर्व इन्द्रिय असमर्थ होजाते हैं, उन दोषों का जो केवल इच्छारूप से रहना है इसी को “एकेन्द्रियवैराग्य” कहते हैं, और दिव्य अदिव्य अर्थात् उत्तम, अधम, विषयों की प्राप्ति होने पर भोग इच्छा के त्याग को “वशीकारवैराग्य” कहते हैं।।
इन चार प्रकार के अपरवैराग्य का भलेप्रकार अनुष्ठान करने से चित्त की राजस, तामस, सर्ववृत्तियें निरूद्ध होकर सम्प्रज्ञात योग की प्राप्ति होती है, इसलिये वह अपरवैराग्य सम्प्रज्ञात योग का अन्तराड. और असम्प्रज्ञात योग का वहिरड. साधन है।।
सं०- अब परवैराग्य का लक्षण करते हैं-