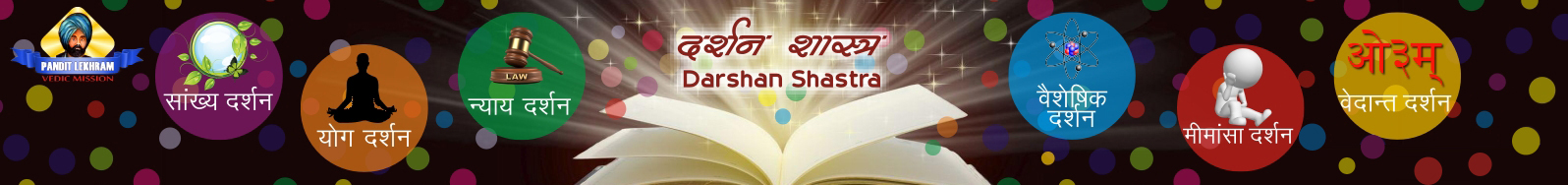सूत्र :तस्याभावादव्यभिचारः 4/1/10
सूत्र संख्या :10
व्याख्याकार : स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती
अर्थ : जिस हेतु से व्यभिचार दोष दिया गया अर्थात् यह बतलाया गया है कि जिस अनेक द्रव्यों के मिले हुए पदार्थ में रूप रहता है उसमें गुरूत्व भी रहता है, इसलिए गुरूत्व का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। परन्तु एक ही अधिकरण में दो गुणों के रहने से यह आवशकता नहीं कि दोनों का प्रत्यक्ष हो। यदि सार्वत्रिक निय होता कि एक ही इन्द्रिय से एक अधिकरण में रहने वाले गुणों का प्रत्यक्ष हो जावे, उस अवस्था में व्यभिचार हो सकता था, परन्तु यह निय ही नहीं, इसलिए व्यभिचार भी नहीं है। और गुरूत्व और रूप को एक ही द्रव्य में रहता हुआ जान कर उनके प्रत्यक्ष होने का विचार करना ही अविद्या है। प्रथम तो दोनों का अधिकरण में रहने वाल गुणों का का प्रत्यक्ष हो जावे, उस अवस्था में व्यभिचार हो सकता था, परन्तु यह नियम ही नहीं, इसलिए व्यभिचार भी नहीं है। और गुरूत्व और रूप को एक ही द्रव्य में रहता हुआ जान कर उनके प्रत्यक्ष होने का विचार करना ही अविद्या है। प्रथम तो दोनों का अधिकरण ही एक नहीं क्योंकि रूप तो अग्नि का गुण है गुरूत्व पृथ्वी के आकर्षण से प्रतीत होता है। जब दोनों का अधिकरण ही एक नहीं तो एक अधिकरण कहना बुद्धि को धोखा देने के कारण है। दुसरे एक अधिकरण में रहने वाले दो गुणों का एक इन्द्रियों से प्रत्य नहीं होता। जैसे अग्नि में रूप और गरमी है। परन्तु आंख के रूप का ज्ञान होता है, परन्तु गरमी का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आंख केवल रूप का ग्रहण करती है। यदि गुरूत्व में रूप होता तो आंख उसका ग्रहण कर लेती। परन्तु नियम तो यह है कि गुण हो नहीं सकता। फिर गुरूत्व में गुण रूप गुण कैसे रह सकता है? जब गुरूत्व में रूप नहीं तो उसको किस प्रकार देखते? इसलिये इन बातों के न होने से से व्यभिचार नहीं है। आशय यह है कि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन्हीं का ज्ञान नियम से होता है।