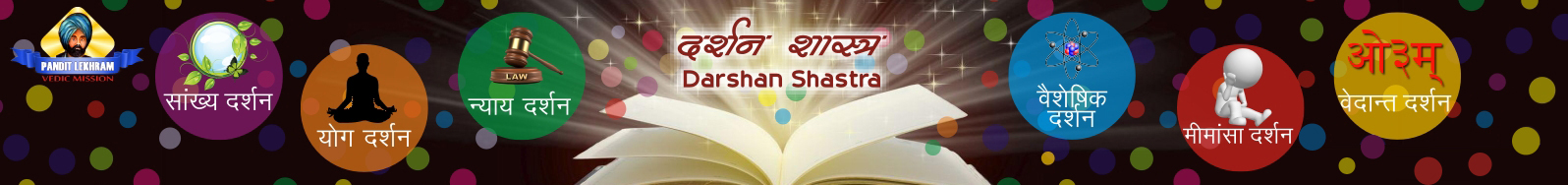सूत्र :प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धेः II2/1/8
सूत्र संख्या :8
व्याख्याकार : स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती
अर्थ : प्रत्यक्षादि का प्रमाण मानना ठीक नहीं क्योंकि इनकी सत्ता अर्थात् प्रमाण होना तीनों काल में प्रमाण को प्राप्त नहीं होता।
व्याख्या :
क्योंकि प्रत्येक प्रमाण का ज्ञान इन तीनों दशाओं से पृथक नहीं हो सकता। प्रथम यह है कि प्रमाण का ज्ञान प्रमेय ज्ञान से प्रथम हो, द्वितीय यह है कि प्रमेय के बोध करने के पश्चात् प्रमाण का ज्ञान हो, तृतीय दशा यह है कि प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान एक ही साथ हो जावे। यहां प्रमाण से प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर उसको शून्य परिमित करने के वास्ते तीनों काल में प्रत्यक्ष का परिमित न होना विपक्षी ने युक्ति उपस्थित की, अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या कारण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण तीनों काल में प्रमाण का प्राप्त नहीं होता, उसके वास्ते विपक्षी अगले सूत्रों में युक्ति उपस्थित करता है। क्योंकि विवादी मनुष्य बिना युक्ति किसी विवाद को नहीं मानते यदि कोई पुरुष यह प्रश्न उपस्थित करे कि बिना युक्ति मानने में क्या हानि है, क्योंकि अल्पज्ञ पुरुष युक्ति से प्रत्येक वस्तु की परीक्षा तो कर ही नहीं सकता, कुछ न कुछ बातें माननी ही पड़ती हैं।परन्तु ऐसा मानने से प्रथम तो मनुष्य की मानन-शीलता जिसके कारण से मनुष्य दूसरे पशुओं से विशेष गिना जाता है और जो कुदरती तौर पर शिशु अवस्था से ही प्राप्त होता है, बिल्कुल हानिकारक है। परन्तु सर्वज्ञ परमात्मा का कोई कार्य हानिकारक नहीं तो उसका मनुष्य की प्रकृति में मननशीलता रखना किसी प्रकार भी हानिकारक नहीं हो सकता। यदि येनकेन प्रकारेण यह मान लिया जाये कि प्रकृति ने मननशीलता मनुष्य की प्रकृति में बिना लाभ रखा तो मनुष्य किसी विषय को सत्यासत्य कह ही नहीं सकता, उस दशा में एक योगी और अज्ञ के कथन पर हठ करने पर किसी को अशुद्व नहीं कह सकते, प्रत्येक को शुद्व मानना पड़ेगा जिससे एक वस्तु की बाबत दो हठ सम्बन्धी सम्मतियों का पक्षी और विपक्षी का मान लेना असम्भव हो जायेगा। इस वास्ते प्रत्येक वस्तु विषयक युक्तियों से परीक्षा करना आवश्यक समक्ष कर अब प्रमाण के शून्य परिमित करने के लिए युक्तियों उपस्थित की जाती है।
प्रश्न - प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमेय ज्ञान के प्रथम मानने में क्या हानि हैं ?