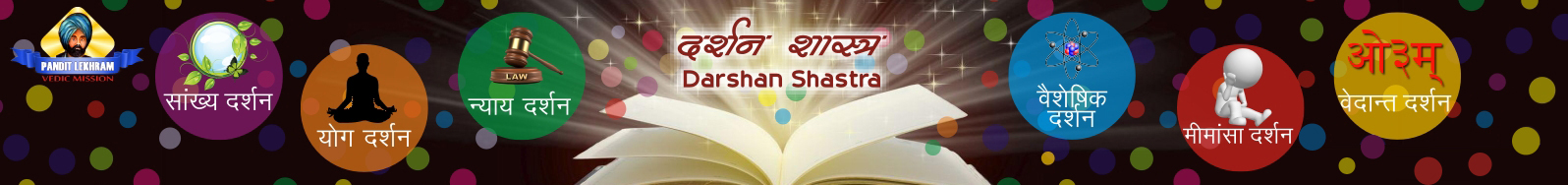सूत्र :शेषः परार्थत्वात् २
सूत्र संख्या :2
व्याख्याकार : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
अर्थ : पाद १ सूत्र २७ तक की व्याख्या
‘शेष’ क्या है? कौन-कौन से कर्म ‘शेष’ हंै। इन सबका वर्णन इस पाद में है।
‘शेष’ का लक्षण हैं ‘शेष: परार्थत्वात्’ (सू० ३.१.२)। शेष वह है जो परार्थ अर्थात् दूसरी चीज के प्रयोजन की सिद्धि करे। जैसे नौकर स्वामी का ‘शेष’ कहलाता है।
यज्ञ में जो चीजें यज्ञ का प्रयोजन सिद्ध करती हैं वे यज्ञ का शेष कहलाती हैं। जैसे द्रव्य, गुण संस्कार! ‘द्रव्य’ वह पदार्थ है जिससे यज्ञ-क्रिया होती है। जैसे आज्य या पुरोडाश या चरु। ‘गुण’ द्रव्य के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण वह द्रव्य यज्ञ में उपकारक होता है। ‘संस्कार’ वह काम है, जिसके करने से द्रव्य उपकार करने के योग्य बन जाता है।
साधारण लौकिक दृष्टान्त यह है। मकान को पोतने के लिये चूना द्रव्य है। सफेदी उसका गुण है। चूने को पानी में डालकर बुझाते हैं यह उसका संस्कार है। ये तीनों मकान की पुताई के शेष हुये। चूना न होता तो पुताई का काम न होता। चूना सफेद न होता तो चूने को क्यों चुनते? यदि चूने को बुझाया न जाता तो चूने का प्रयोग न हो सकता।
याग, फल और पुरुष को कुछ आचार्यों ने ‘शेष’ नहीं माना। कुछ ने माना है। वृत्तिकार ने इस विरोध का समाधान इस प्रकार किया है कि ‘यज्ञ’ को प्रधान मानने पर तो द्रव्य, गुण और संस्कार ही वास्तविक ‘शेष’ हैं। क्रिया, फल और कर्ता की शेषता तो सापेक्षिक है।
जैसे यज्ञ द्रव्य की अपेक्षा प्रधान है। फल की अपेक्षा शेष है। क्योंकि यज्ञ फल का साधक है। फल यज्ञ की अपेक्षा प्रधान है परन्तु यजमान की अपेक्षा शेष है क्योंकि फल यजमान के लिये होता है। कर्ता या यजमान फल की अपेक्षा प्रधान है। परन्तु यजमान यूप को नापता है अत: यहां वह यूप का शेष हुआ।
अब यज्ञ-विधान की श्रुतियों का उदाहरण देकर बताया है कि कौन कर्म किसका शेष है। क्योंकि नियम यह है कि जो चीज जिस दूसरी चीज का उपकार करे वह उसी का शेष है। जैसे सभी नौकर सभी स्वामियों के नहीं होते इसी प्रकार सब शेष सभी प्रधानों के उपकारक नहीं होते। कौन किसका शेष है यह जानना यज्ञ के सम्पादन के लिये अत्यावश्यक है। यह उदाहरण लीजिये—
(१) कुछ संस्कार हैं। यह उन-उन चीजों के शेष हैं। जैसे—
(अ) निर्वपन (धान को निकालना), प्रोक्षण (धोना), अवहनन (कूटना)।
(आ) उत्पवन (छाछ में से नवनीत या लौनी निकालना), विलापन (पिघलाना), ग्रहण (पात्र में निकालना) आसदन (वेदी पर लाकर रखना)।
(इ) सान्नाय्य या दधि मिश्रित दूध के बनाने के लिए ये संस्कार किये जाते हैं—शाखा हरण (वृक्ष की टहनियों को तोडऩा), गवां प्रस्थापनम् (उन शाखाओं से गायों को हांककर लाना), गवां प्रस्तावनम्् (गायों को दूहना आदि)।
ये संस्कार हैं ओषधि, आज्य और सान्नाय्य के, इसलिये यह शेष हुये। (देखो सू० ६-१०)
(२) यज्ञ के दस आयुध या साधन गिनाये—(१) स्फ्या (खोदने की खुरपी), (२) कपाल (पकाने के तवे), (३) हवणी (आहुति देने की चमची), (४) सूप (चावल फटकने की चीज), (५) कृष्णार्जन या मृगछाला (जिस पर ओखली रखते हैं), (६) शम्या (चक्की की कीली), (७) ओखली, (८) मूसल (कूटने के लिये), (९) दृषद् (नीचे का पाट), (१०) उपल (ऊपर का पाट, पीसने के लिये)। ये अपने-अपने काम के शेष हैं।
(३) कभी-कभी द्रव्य और गुण एक ही वाक्य में किसी एक काम की सिद्धि करते हैं, उस दशा में वे दोनों उसी काम के ‘शेष’ हैं। जैसे ‘अरुणया पिंगलाक्ष्या एकाहन्या सोमं क्रीणाति’ (तै०सं० ६.१.६.७) अर्थात् एक लाल, पिंगल, आंख वाली, एक वर्ष की गाय के बदले सोम को खरीदता है।’ यहां ‘लाल’ एक गुण है। गाय एक द्रव्य है। ये दोनों ‘शेष’ हैं सोमक्रय के। अरुण का अर्थ है अरुण गाय। अर्थात् सोमक्रय के योग्य गाय। चाहे वह अरुण न भी हो।
(४) कहीं-कहीं द्रव्य तो कई होते हैं। परन्तु उनमें से एक के ही संस्कार का विधान कथित होता है। वहां ऐसा समझना चाहिये कि वह संस्कार उन सभी द्रव्यों पर लागू होता है, अत: सभी का ‘शेष’ है। जैसे ‘दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्र्टि’ (पवित्रे से ‘ग्रह’ को मांजता है)। यहां ग्रह एक वचन है। परन्तु सभी ग्रह मांजने चाहियें। अर्थात् ‘मांजना’ संस्कार सभी ग्रहों का शेष है। केवल एक ग्रह का नहीं।
‘अग्नेस्तृणान्यपचिनोति’ अर्थात् वेदी के तिनके बटोरता है। यहां ‘अग्ने:’ (वेदी का) एक वचन है। परन्तु तिनके सभी वेदियों के बटोरने हैं जिससे सब वेदियां साफ हो जायं, यह ‘सफाई’ रूपी संस्कार सब वेदियों का है।
‘पुरोडाश पर्यग्निं करोति’ अर्थात् पुरोडाश को अग्नि पर रखकर सेंकता है। यह ‘सेंकने’ का संस्कार सभी पुरोडाशों के लिये करना है अत: सब का शेष है। (देखो सू० १३-१५)
हां! एक बात का ध्यान रखना चाहिये। वे सब पदार्थ एक ही कोटि के होने चाहियें। यदि भिन्न-भिन्न कोटियों के हों, तो नहीं। जैसे ग्रहों के मांजने का विधान है। चमसों का नहीं। अत: विधान के अनुसार चमसों का मांजना अभिप्रेत नहीं हैं। क्योंकि ग्रह पात्र भिन्न होते हैं और चमस पात्र भिन्न। श्रुति में विधान ‘ग्रह’ मांजने का है। अत: ‘मांजना’ चमसों का शेष नहीं होगा (देखो सू० १६-१७)
(५) कभी-कभी एक संस्कार किसी मुख्य कर्म का उपकारक नहीं होता अपितु उसके अंग का होता है। फिर भी उसको मुख्य कर्म का शेष कहते हैं। जैसे देवदत्त का पोता उसके पुत्र की सन्तान है फिर भी देवदत्त की सन्तान कहलाता है। इसका यज्ञसम्बन्धी उदाहरण यह है—
सप्तदशारत्निर्वाजपेयस्य यूपो भवति अर्थात् वाजपेय यज्ञ के यूप की ऊंचाई १७ हाथ हो। वाजपेय याग में यूप होता ही नहीं। वाजपेय का एक अङ्ग है ‘पशुयाग’। उसमें यूप होता है। अत: १७ की संख्या वस्तुत: शेष है पशुयाग की। परन्तु मानी गई है मुख्य याग अर्थात् वाजपेय की।१
(६) कभी-कभी एक कर्म पूरे याग का शेष न होकर केवल एक अङ्ग का ही शेष होता है। क्योंकि उस कर्म से केवल उसी अङ्ग की आकाङ्क्षा (कमी) पूरी नहीं होती है। इसका एक उदाहरण यह है—
‘अभिक्रामं जुहोति अभिजित्यै’ (तै०सं० २.६.१.४)
इस वाक्य का आशय है कि आगे बढक़र आहुति देता है। यहां ‘अभिक्रामं’ यह णमुल् है। अर्थात् दूसरी क्रिया की अपेक्षा रखता है। ‘जुहोति’ क्रिया से यह प्रतीत होता है कि ‘अभिक्रमण’ कर्म का सम्बन्ध समस्त याग से है। परन्तु वस्तुत: स्थिति दूसरी ही है। यहां प्रकरण प्रयाजों का था। पहले ऐसा वाक्य है ‘अतिहायेडो बर्हि: प्रति समानयते जुहुवामौपभृतम्।’ यहां बर्हि या कुश प्रयाज के लिये ही लाया गया था। इसके पीछे ‘अभिक्रामं जुहोति’ ऐसा कहा फिर कहा ‘प्रयाजशेषेण हवींष्यभिधारयति।’ इस प्रकार पूर्वापर के सम्बन्ध से यह सिद्ध हुआ कि ‘अभिक्रामण’ का सम्बन्ध केवल प्रयाजों से है। अर्थात् ‘प्रयाजों’ की आहुतियां आगे बढक़र देनी हैं। यहां ‘अभिक्रमण’ कर्म प्रयाजों का शेष है, पूरे याग का नहीं।१
(७) परन्तु ‘उपवीत’ समस्त याग का शेष है क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता।२
शंका इसलिये हुई कि प्रकरण में पहले काम्य साभिधेनियों का वर्णन था फिर उपवीत का। अत: भ्रम से यह समझ लिया गया कि जैसे अभिक्रमण केवल एक अङ्ग अर्थात् प्रयाजों का ही शेष है इसी प्रकार ‘उपवीत’ भी केवल काम्य सामिधेनियों का शेष होगा। परन्तु सामिधेनियों का प्रकरण तो पहले ही समाप्त हो गया। अत: ‘उपवीत’ समस्त याग का शेष है।
(८) यदि दो कर्म जो समकक्ष हैं किसी एक प्रधान कर्म के अङ्ग हों तो वह परस्पर एक दूसरे के अंग नहीं होते। लौकिक दृष्टान्त यह है कि कान और नाक शरीर के अङ्ग हैं। परन्तु कान और नाक एक दूसरे के अङ्ग या अङ्गी नहीं, इसी प्रकार सामिधेनी मंत्र और निविद मंत्र दोनों अग्नि की स्तुति के लिये होने से यज्ञ के अंग हैं। परन्तु परस्पर एक-दूसरे के अंग नहीं।
इसी प्रकार पवमानहवि और अग्न्याधेय ये दोनों अग्नि के गुण हैं। क्योंकि अग्न्याधेय कर्म से भी अग्नि का संस्कार होता है और पवमान हवि से भी। अत: वे दोनों आपस में अंग अंगी नहीं। इसलिये वारण और वैकङ्कट पात्रों का सम्बन्ध पूरे यज्ञ से है। नीचे की दो श्रुतियों को देखिये—
(अ) तस्माद् वारणो वै यज्ञावचर: स्यान् न त्वेतेन जुहुयात्। वैकङ्कतो यज्ञावचर: स्यात्। जुहुयादेतेन।
(आ) यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीष्ट: प्रीतो भवति।
यहां यह दोनों पात्र, वारण और वैकङ्कत यज्ञावचर अर्थात् यज्ञ के लिये हैं। अङ्गों के लिये नहीं।
(९) वात्र्रघ्नी-न्याय—जैसे ‘देहल-दीपक-न्याय’, ‘अन्धचटुक न्याय’ आदि हैं, इसी प्रकार ‘वात्र्रघ्नी-न्याय’ है।
‘वात्र्रघ्नी-न्याय’ यह है कि जिस क्रम से मंत्र दिये हैं उसी क्रम से उनका अङ्ग-अङ्गी भाव भी है। ‘वात्र्रघ्नी’ शब्द का अर्थ है वे दो ऋचायें जिन में वृत्र को मारनेवाले वृत्रहा इन्द्र का वर्णन है। ये दो मंत्र पौर्णमास-इष्टि के दो आज्य भागों की अनुवाक्यायें हैं पहली ऋचा ऋग्वेद ६.१०.३४ है। दूसरी ऋग्वेद १.९१.५ इन दोनों में वृत्र को मारने का कथन है।१
इसी प्रकार दो और अनुवाक्यायें हैं। जिनको ‘वृधन्वती’ कहते हैं। ऋग्वेद ८.४४.१२ और ऋ०वे० १.९१.११। इनमें ‘वृद्धि’ शब्द आया है। अत: इनका नाम वृधन्वती हैं। यह अमावास्या-इष्टि के आज्यभागों की अनुवाक्या हैं।
प्रश्न यह था कि यह चारों अनुवाक्यायें प्रधान-इष्टि अर्थात् दर्शपूर्ण मास के अङ्ग हैं अथवा उनके अन्तर्गत आज्यभाग आहुतियों के। क्योंकि विधिवाक्य इस प्रकार है—
वात्र्रघ्नी पौर्णमास्यायामनूच्येते, वृधन्वती अमावा-स्यायाम्। (तै०सं० २.५.२.५)
+
‘वात्र्रघ्नी न्याय’ यह है कि इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं। यह दोनों (वात्र्रघ्नी और वृधन्वती) अलग-अलग हैं। इनके देवता भी अलग हैं और कर्म भी अलग हैं। अत: यह प्रधान याग के अङ्ग नहीं, आज्यभागों के अङ्ग हैं। (देखो सू० ३.१.२३)
(१०) ऊपर के सिद्धान्त के विपरीत भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में तीन कर्म दिये हैं—(अ) मुष्टी करोति= मु_ी बांधता है। (आ) वाचं यच्छति=मौन रहता है। (इ) दीक्षित-मावेद्यति=यह घोषित करता है कि मैं दीक्षित हूं।
इसी प्रकार दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में दो कर्म दिये हैं—(क) हस्तौ आनेनक्ति=हाथों को धोता है। (ख) उलपराजिं स्तृणाति= कुशों को बिछाता है। यहां प्रश्न यह है कि क्या पहले तीन कर्म ज्योतिष्टोम के अंग हैं या इनमें से पहले दो, तीसरे के हैं अर्थात् क्या मु_ी बांधना और मौन रखना केवल अपने को दीक्षित घोषित करने के लिये था या समस्त याग के लिये। ऊपर दिये ‘वात्र्रघ्नी न्याय’ से तो पहले दो कर्मों को तीसरे का अङ्ग मानना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है। ये तीनों काम अलग-अलग हैं। एक-दूसरे में अङ्ग-अङ्गी भाव नहीं है, अत: ये तीनों अङ्ग हैं पूरे याग के।
इसी प्रकार क और ख कर्मों को भी प्रधान याग का अङ्ग मानना चाहिये। यह नहीं समझना चाहिये कि कुशों को बिछाने के लिये हाथ धोये हैं। (देखो सू० २४, २५)
(११) ‘लक्षणार्था गुणश्रुति:’ अर्थात् यदि श्रुति में गुण दिया हो तो उसका प्रयोजन देखकर निर्णय करना चाहिये कि कौन किसका अंग है।
श्रुति में दिया है, ‘आग्नेयं चतुर्धा करोति’=आग्नेय पुरोडाश के चार भाग करता है। पुरोडाश तो ‘आग्नेय’ भी होता है, अग्नीषोमीय भी और ऐन्द्राग्नि भी। अग्नि शब्द तीनों में पड़ा है और ‘अग्नि’ देवता का तीनों में उल्लेख है। प्रश्न यह था कि इन सबके पुरोडाशों के चार-चार भाग होंगे या इस विधिवाक्य के अनुसार केवल आग्नेय पुरोडाश के। सिद्धान्त यह है कि केवल ‘आग्नेय’ के। ‘अग्नीषोमीय’ और ‘ऐन्द्राग्नि’ पुरोडाशों का नाम आग्नेय नहीं हैं, क्योंकि इनमें सोम और इन्द्र भी मिश्रित हैं। इसलिये चार भाग करने का काम आग्नेय पुरोडाश का ही शेष है। अन्यों का नहीं।१