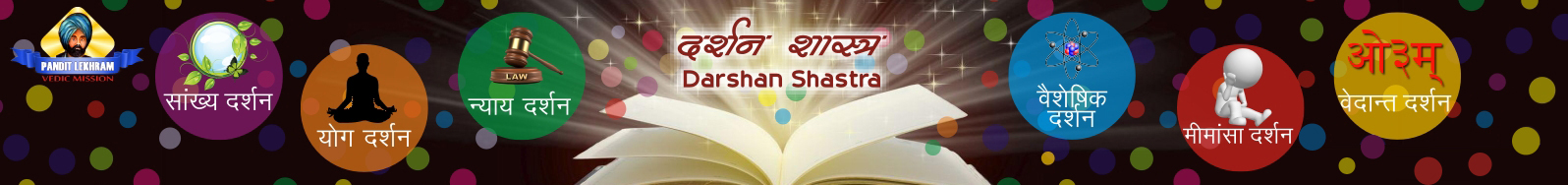सूत्र :नार्थपृथक्त्वात् ७
सूत्र संख्या :7
व्याख्याकार : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
अर्थ : पाद ३ सूत्र १ स्व ४१ तक की व्याख्या
इस पाद में उदाहरण देकर यह बताया है कि द्रव्य, संस्कार तथा अन्यान्य क्रियायें स्वयं अपना फल नहीं देतीं। फल तो प्रधान कर्म का ही होता है। ये तो उस कर्म के सहायक मात्र हैं। अत: यदि किसी श्रुति में उनका विशेष फल दिया हो तो वह केवल अर्थवाद है। वास्तविक फल नहीं। जैसे—
(१) खदिर का स्रुवा हो तो आहुतियां रसवाली हो जाती हैं। या जुहू पर्णमयी (पलाश की) हो तो पाप-श्लोक नहीं सुनता। यह द्रव्यों के फल बताये (२) जो आंख में अंजन लगाता है वह शत्रु की आंख में खटकता है। यह संस्कार का फल बताया। या (३) कुछ उपकर्म हैं जैसे दो आज्यभाग आहुतियां यज्ञ की दो आंखें हैं। यह सब क्रत्वर्थ है, पुरुषार्थ नहीं। इनका फल अलग नहीं है। ऊपर बताये फल केवल अर्थवाद हैं। उत्साह दिलाने के लिये कह दिये गये। (सू० १-३)
कुछ ऐसी चीजें या संस्कार या क्रियायें हैं जो विकार-यज्ञों से सम्बन्ध रखते हैं। विकार का अर्थ है वि+करण१ अर्थात् विशेष इष्टियों में, इनका नित्य प्रयोग नहीं समझना चाहिये। अर्थात् उनका प्रयोग उन्हीं विशेष अवस्थाओं के लिये है। इसके तीन दृष्टान्त भाष्यकार ने दिये हैं। (१) यदि ब्राह्मण यजमान हो तो ‘बार्हद्गिर’ नामी ब्रह्म साम गाया जावे, यदि क्षत्रिय हो तो पार्थुरश्म साम, यदि वैश्य हो तो रायोवाजीय साम, (२) अग्न्याधान के लिये जो वेदी बनाते हैं वह पहली बार १००० ईंटों की दूसरी बार २००० ईंटों की, तीसरी बार ३००० ईंटों की बनानी चाहिये। (३) यदि यज्ञ पशु की कामना से किया जाय तो प्रणीता जलों को दुहनी में लावें, यदि ब्रह्मवर्चस् चाहें तो कांसे के पात्र में, यदि प्रतिष्ठा चाहें तो मिट्टी के पात्र में। ये शर्तें विशेष अवस्थाओं के लिये हैं, सब कामों के लिये नहीं। (सू० ३-४)
कहीं-कहीं संयोग-पृथक्त्व न्याय से जब एक ही चीज नित्य कर्मों के सम्बन्ध में कही जाती है तो उसका प्रयोग सर्वत्र होता है परन्तु जब उसके साथ एक विशेष शर्त लगा दी जाती है तो उसको अन्य स्थानों पर नहीं ला सकते। इसके उदाहरण ये हैं—(१) पहले कहा ‘दध्ना जुहोति’ अर्थात् दही की आहुति देता है। दूसरे स्थान पर कहा ‘दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्’ अर्थात् इन्द्रिय बल की कामना वाला दही की आहुति दे। यहां पहले वाक्य में संयोग है अत: दही सब यज्ञों के लिये कथित है। दूसरे वाक्य में पृथक्त्व है अर्थात् जहां इन्द्रिय की कामना न हो वहां दही का प्रयोग न होगा। (२) यूप खदिर का हो।
अन्यत्र कहा, वीर्य की कामना वाले के लिये खदिर का यूप बनाना चाहिये। (सू० ५-७)
ज्योतिष्टोम में बताया है कि ब्राह्मण दूध पीकर रहे, क्षत्रिय यवागू खाकर और वैश्य आमिक्षा खाकर (तै०सं० ६.२.५.२-३)। ये व्रत क्रत्वर्थ हैं। क्योंकि यज्ञ करने में इनसे सुगमता होती है। इनका अपना कोई फल नहीं। (सू० ८,९)
अब यहां दो यज्ञों का दृष्टान्त देकर उन्हीं यज्ञों के नाम पर दो न्यायों का उल्लेख करते हैं। एक ‘विश्वजित् यज्ञ’ है जिसके नाम पर ‘विश्वजित्-न्याय’ पड़ा। दूसरा ‘रात्रि सत्र’ है जिसके नाम पर रात्रि-सत्र न्याय पड़ा।
विश्वजित् यज्ञ के विधिवाक्य में फल का कथन नहीं है। रात्रि सत्र के विधिवाक्य में फल भी दिया है। कोई यज्ञ बिना फल के तो होता नहीं। अत: विश्वजित् यज्ञ का भी फल होता है और एक ही फल होता है अर्थात् स्वर्गप्राप्ति। इसलिये जिन यज्ञों में फल न दिया हो उनका विश्वजित्-न्याय से स्वर्ग फल मान लेना चाहिये।
रात्रि सत्र में स्वर्ग फल मानने की आवश्यकता नहीं। वहां तो फल दिया ही हुआ है। ‘प्रतितिष्ठति ह वा य एता रात्रीरूपयन्ति। ब्रह्मवर्चस्विनोऽन्नादा भवन्ति य एता उपयन्ति।’ अर्थात् रात्रि सत्र का फल है प्रतिष्ठा, ब्रह्मवर्चस, अन्नाद्य आदि यह अर्थवाद नहीं है। क्योंकि ‘द्रव्य संस्कार कर्मसु’ फल का कथन अर्थवाद कहते हैं (सू० १) ऐसे वाक्य अर्थवाद नहीं हो सकते। (१०-१९)
कुछ काम्य इष्टियां हैं जैसे ‘सौर्य चरुं निर्वपेद् ब्रह्मवर्चसकाम:’ (तै०सं० २.३.२.३) यहां ब्रह्मवर्चस् की कामना के लिये सौर्य-इष्टि का कथन है। अत: यहां स्वर्ग-फल की कल्पना व्यर्थ है। काम्य इष्टियों का वही फल होता है जो विधि वाक्यों में दिया है। (सू० २०-२४)
परन्तु दर्शपूर्णमास और ज्योतिष्टोम से सभी फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये श्रुतियां हैं—(१) एकस्मै वाऽन्या इष्टय: कामायाऽऽ-ह्रियन्ते, सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ। (२) एकस्मै वाऽन्ये कामायाऽऽ-ह्रियन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोम:। अर्थात् अन्य इष्टियों के तो एक-एक फल ही होते हैं दर्शपूर्णमास और ज्योतिष्टोम तो सभी फलों का दाता हैं। (सू० २५-२६)। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि एक बार दर्शपूर्ण-मास या ज्योतिष्टोम करने से एक साथ सभी फल मिल जायेंगे। वस्तुत: न सब कामनायें एक साथ उत्पन्न होती हैं न एक कर्म से पूरी होती हैं। श्रुति में भी यह नहीं कहा कि एक साथ ही सब फलों की प्राप्ति होगी। तात्पर्य यह है कि जिस-जिस कामना से इन यज्ञों का अनुष्ठान होगा। उसी-उसी फल की पूॢत होगी। कुछ की इस जन्म में भी और कुछ की दूसरे जन्म में। जो लोग यह समझते हैं कि इस जन्म में फल मिलता ही नहीं वह ठीक नहीं ‘इहैवैषां सिद्धिर्योगस्य।’ (सू० २८ और भाष्य)१ इसी जन्म में फल मिल सकता है यदि पहले जन्म के कर्म बाधक न हों। यदि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म बचे हैं जो इस जन्म के कर्मों में बाधक हो सकते हैं तो वह फल रुक सकता है परन्तु मिलेगा अवश्य।
अब यहां कुछ ऐसे यज्ञों के उदाहरण हैं जो दूसरे यज्ञों के अंग हैं—(१) सौत्रामणि अग्नि का अंग है। (२) बृहस्पति-सत्र, वाजपेय का अङ्ग हैं। (३) वैमृद्ध इष्टि पौर्णमास का अङ्ग है। (सू० ३१-३५)
कुछ ऐसे भी हैं जो अङ्ग नहीं है। जैसे—
(१) अग्नि मारुत यज्ञ के पश्चात् अनुयाज आहुतियां अग्नि मारुत का अङ्ग नहीं, (२) दर्शपूर्णमास के पश्चात् सोम यज्ञ किये जाते हैं। वे भी दर्शपूर्णमास के अङ्ग नहीं केवल समय का सम्बन्ध है।
(सू० ३६,३७)।
वैश्वानर-इष्टि का फल पुत्र को मिलता है। वह पुत्र के लिये ही की जाती है। इसको जातकर्म के पश्चात् अशौच काल के पीछे करना चाहिये। (सू० ३८, ३९) देखो—वैश्वानरं द्वादश कपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते। यस्मिन् जाते एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव स तेजस्वी अन्नाद: इन्द्रियावी, पशुमान् भवति। (तै०सं० २.२.५.४)। यहां दो बातें दी हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर वैश्वानर करे। उसके कहने का यह फल होगा कि पुत्र तेजस्वी, अन्नाद आदि होगा।
सौत्रामणि आदि अङ्गों को समय पर ही करना चाहिये।
(सू० ४०-४१)।