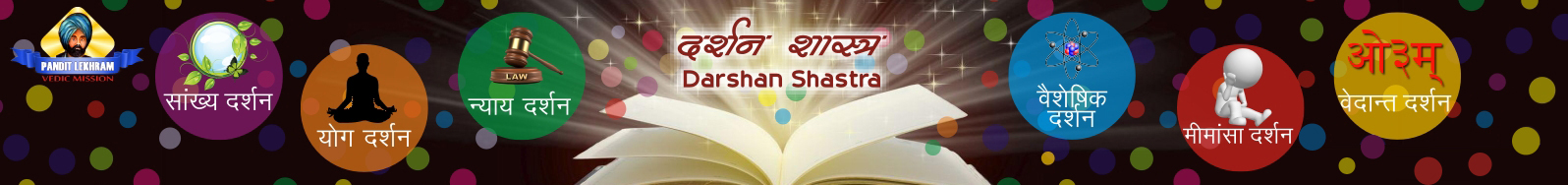सूत्र :विधेः कर्मापवर्गित्वादर्थान्तरे विधि-प्रदेशः स्यात् २९
सूत्र संख्या :29
व्याख्याकार : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
अर्थ : पाद २ सूत्र १ से ३० तक की व्याख्या
गत पाद में आमिक्षा और वाजिन् का दृष्टान्त देकर यह समझाया गया था कि एक क्रिया से जो दो चीजें उत्पन्न हो जायें उनमें मुख्य वही है जिसके उद्देश्य से क्रिया की गई थी, अन्य नहीं।
इस पाद में यह बतायेंगे कि क्रिया तो एक विशेष वस्तु के लिये की जाती है परन्तु उसके साथ अप्रधान चीज भी बन जाती है उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण ये हैं—
(१) ‘ज्योतिष्टोम यज्ञ’ के अग्नीषोमीय पशु के लिये खदिर आदि लकड़ी का यूप बनाते हैं, यूप छीलने में जो पहला छिल्लड़ निकलता है। उसे ‘स्वरु’ कहते हैं क्योंकि वह स्वयं यूप से काटा जाता है, (स्वमिवारुर्भवति। शतपथ ब्रा० ३.७.१.२४)। उस स्वरु से पशु को चुपड़ते हैं। (स्वरुणा पशुमनक्ति)। यहां लकड़ी के छीलने का प्रधान प्रयोजक तो ‘यूप’ ही था। स्वरु उसी का टुकड़ा है। वह तो अप्रधान रूप से बन गया है। अत: उससे एक काम ले लिया गया। (सू० १६)१
(२) बछड़ों और गायों को हांकने के लिये एक शाखा काटी जाती है। उसके दो टुकड़े करते हैं। नीचे का मोटा ६ इञ्च लम्बा भाग उपदेश कहलाता है। इससे चिमटे का काम लिया जाता है जैसे आग कुरेदना, कपालों का आग पर रखना। शेष ऊपर के पहले भाग से बछड़ों, गायों आदि को हांकने का काम लेते हैं। यहां शाखा प्रधान प्रयोजन है। उपवेश लकड़ी काटने का प्रयोजक नहीं? अप्रधान है, (सू० ८)
इसी सम्बन्ध में शाखा का महत्त्व बताते हैं। ‘प्राचीमाहरति उदीचीमाहरति। प्रागुदीचीमाहरति।’ यहां साधारण अर्थ तो हुआ पूर्व दिशा को लाता है, उत्तर दिशा को लाता है इत्यादि। परन्तु दिशायें तो लाई नहीं जा सकतीं। अत: ठीक अर्थ यह है कि शाखा को वेदी के पूर्व दिशा में लाता है इत्यादि। यहां ‘शाखा’ प्रधान है, (सू० ४.२.७)२
अब प्रतिपत्ति कर्म लेते हैं। किसी चीज से दो कर्म लिये जाते हैं। एक तो ‘अर्थ कर्म’ अर्थात् वह काम जिसके लिये मुख्यतया वह चीज प्राप्त की गई। जैसे शाखा लाने का उद्देश्य था बछड़े हांकना। यह ‘अर्थ कर्म’ है। जब वह कर्म होगया तो उसको कूड़े में फेंक देना चाहिये। परन्तु याग की पवित्र भावना के रखने के लिये ऐसा नहीं करते। एक विधि द्वारा आग में डाल देते हैं। इस संस्कार का नाम है ‘प्रतिपत्ति कर्म’ लगभग (अन्त्येष्टि-संस्कार के समान)। एक उदाहरण है—
(क) ‘सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति।’ यहां प्रस्तर या कुश के गुच्छे को तो आग में डालना ही था, वह प्रतिपत्ति कर्म न था, परन्तु उसके साथ शाखा को भी आग में डाल देना प्रतिपत्ति कर्म है। (सू० १०)
(ख) इसी प्रकार यज्ञों में जो जल लाये जाते हैं उनका नाम है ‘प्रणीता’। इनका ‘अर्थ कर्म’ तो है आटा गूंधना आदि।
आटा गूंधने का नाम है ‘संयवन’। जल फेंकने का नाम है ‘निनयन।’
(ग) ‘क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति’ (तै०सं० ६.१.४.१-२)। यहां सोम के खरीदने के पश्चात् ‘मैत्रावरुण’ नामक ऋत्विज् को ‘दण्ड’ थमाने का विधान है। यह अर्थ कर्म है, प्रतिपत्ति कर्म नहीं। दण्ड बिना कारण उसको थमा नहीं दिया गया। यज्ञ में उसका आगे काम पड़ेगा। जैसे ‘दण्डी प्रैषानन्वाह’। यहां मैत्रावरुण को ‘दण्डी’ कहा क्योंकि दण्ड हाथ में लेकर ‘प्रैष’ आज्ञाओं को देना चाहिये। (सू० १६-१८)
(घ) यज्ञशाला में एक जलगृह या स्नानागार होता है। उसका नाम है ‘अवभृथ’। यज्ञ के पश्चात् कई चीजें होती हैं जिनमें सोम लगा रह जाता है, जैसे ऋजीष या डण्ठल जिनसे सोम लिया गया। ग्रावाण या पत्थर जिन पर सोम कुचला गया, उदुम्बर की लकड़ी, दो पत्थर की पट्टियां जिन पर सोम पीसा गया। इन सबको हटाकर ‘अवभृथ’ में रख देते हैं। यह प्रतिपत्ति कर्म है। अर्थ कर्म नहीं। (सू० २०-२२)
श्रुतियों में जहां यज्ञ के कर्ताओं, देश या काल का विधान है वहां यह विधान ‘नियमन’ अर्थात् मर्यादा बांधने के लिये है। अर्थवाद नहीं है। नियमन के कुछ उदाहरण यह हैं—
(अ) पशुबन्ध में ६ ऋत्विज् होते हैं। दर्शपूर्णमास में चार, चातुर्मास्य में ५, अग्निहोत्र में १, सोमयाज में १७ (यह हुआ कर्ताओं की संख्या का नियमन)। इसी दर्शपूर्णमास को समतल भूमि पर करे। वैश्वदेव यज्ञ की भूमि पूर्व की ओर ढालू हो। (यह हुआ स्थान का नियमन)। पौर्णमास-इष्टि पूर्णमासी की तिथि को करे। दर्श-इष्टि अमावास्या को। (यह हुआ समय का नियमन)। (देखो तै०ब्रा० २.३.५.१-४ तथा भाष्य सहित सूत्र २२-२४)।
(आ) इसी प्रकार द्रव्यों का भी नियमन है। जैसे ‘वायव्यांश्वेत-मालभेत भूतिकाम:’ (तै०सं० २.१.१.१) अर्थात् ऐश्वर्य की कामना वाला वायु देवता के लिये श्वेत पशु का आलभन करे। (यहां पशु का नियमन है)। ‘सोमा रौद्रं छते चरुं निर्वपेच् छुल्कानां व्रीहीणां ब्रह्मवर्चसकाम:।’ (मै०सं० २.१.५) नैऋतं चरुं निर्वपेत् कृष्णानां व्रीहीणाम्। (तै०सं० १.८.९.१)=यहां सोमा रौद्र चरु के लिये सफेद चावलों और निर्ऋति के चरु के लिये काले चावलों का विधान नियमन के लिये है। (सू० २५)
(इ) व्रीहीन् अवहन्ति, तण्डुलान् पिनष्टि। (धान कूटता है, चावल पीसता है)। यह संस्कार भी नियमन अर्थात् मर्यादा बांधने के लिये है। (सू० २६)
अब तक शेष या अंग के लक्षण बताये। अब यह बताते हैं कि प्रधान कर्म क्या है जिसके ये शेष या सहायक थे। जिनमें यजति (यज्ञ करना), ददाति (दान देना) जुहोति (होम करना) ये तीन लक्षण हों वह प्रधान कर्म है, अर्थात् याग, दान और होम। जिस कर्म में द्रव्य और देवता का सम्बन्ध स्थापित किया जाय वह ‘याग’ कहलाता है। इन सब प्रधान कर्मों में ‘यजति’ शब्द का प्रयोग होता है। जिस अर्थ में ‘याग’ शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें ‘होम’ भी है। आहुतियां देना अधिक है। अपना स्वत्व छोडक़र दूसरे को स्वत्व देना ‘दान’ है। याग, होम और दान१ इन तीनों में उत्सर्ग या अर्पण करना समान है। याग, दान और होम में क्या भेद है? ‘प्रभाकर मीमांसा’ में दिया है कि याग में केवल मौखिक या संकल्प मात्र उत्सर्ग होता है। क्योंकि देवता द्रव्य को कहीं उठा नहीं ले जाते। होम में अग्नि में आहुति दी जाती है। दान में चीज दूसरे की हो जाती है। अत: त्याग भाव तो सभी में है। भट्ट भास्वर का कथन है कि हर होम में आग में आहुति नहीं दी जाती। कहीं कहीं पानी में भी दी जाती है जैसे अवभृथ-इष्टि में। (सू० २८)
अन्त में यह बात यह बताई गई कि बॢह या कुश ज्योतिष्टोम की तीनों इष्टियों में समान रूप से सम्बन्धित रहते हैं। उनका लवन या काटना तीनों इष्टियों के लिये समान प्रयोजन रखता है। ज्योतिष्टोम में तीन इष्टियां होती हैं उनका नाम ‘उपसद’ इष्टियां हैं। औपवस्थ के दिन तीसरी अर्थात् अग्नीषोमीय इष्टि होती है। इन तीनों में एक ही बॢह या कुशों का प्रयोग होता है।