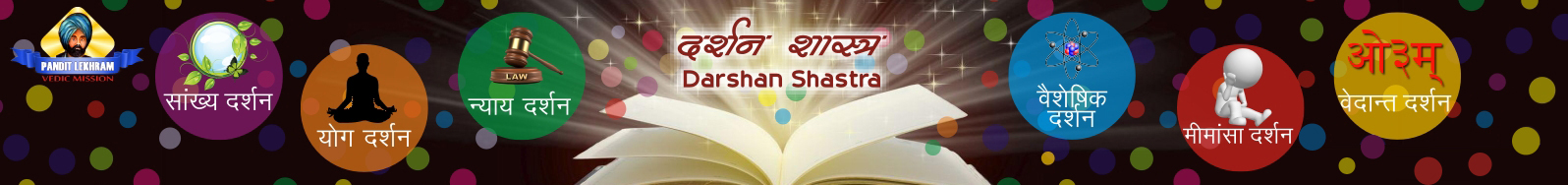व्याख्याकार : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
अर्थ : पाद १ सूत्र ४९ तक की व्याख्या :
अध्याय २, पाद १
पहले अध्याय में इतनी बातें बता दी गई—
(१) प्रमाण का लक्षण अर्थात् धर्म को कैसे पहचाना जाय।
(२) विधि, अर्थवाद, मन्त्र तथा स्मृति की परीक्षा की गई।
(३) गुण-विधि और नामधेय की विवेचना की गई।
(४) यह भी बताया गया कि जहां अर्थों में सन्देह हो वहां वाक्य शेष की सहायता लेनी चाहिये।
अब दूसरे अध्याय में यह बताया जायेगा कि दो यज्ञों के बीच यह कैसे निश्चय हो कि यह यज्ञ प्रधान है और यह अप्रधान और एक यज्ञ दूसरे यज्ञ से भिन्न है या नहीं।
पहले ‘अपूर्वं’ शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिये क्योंकि अपूर्व की अपेक्षा से ही यज्ञों की भिन्नता जानी जाती है। मीमांसा में ‘कर्म’ शब्द का वही अर्थ है जो यज्ञ का। यज्ञ किसी फल की प्राप्ति के लिये किये जाते हैं जैसे ‘स्वर्गकाम: यजेत’ अर्थात् स्वर्ग की कामना करे उसे यज्ञ करना चाहिये। यज्ञ तो अभी समाप्त हो जायेगा। स्वर्ग मिलेगा मृत्यु के पश्चात्। कैसे माना जाय कि यज्ञ का फल स्वर्ग है? मीमांसा शास्त्र में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यज्ञ से एक अदृष्ट शक्ति उत्पन्न होती है जिसे अपूर्व कहते हैं। यह अपूर्व अपने समय पर फल को उत्पन्न करता है। इस प्रकार पहले तो कर्म का अपूर्व होता है और फिर अपूर्व द्वारा फल।२ ‘अपूर्व’ शब्द मीमांसा शास्त्र में बहुत आयेगा। उसके अर्थ पर ध्यान रखना चाहिये। कर्म और फल के बीच में ‘अपूर्व’ एक माध्यम है। उसको ‘अदृष्ट’ भी कहते हैं। अपूर्व, नियोग और अदृष्ट ये जटिल शब्द हैं जिनकी मीमांसा के आचार्यों ने जटिल व्याख्याएं की हैं, शबर स्वामी का अपूर्व, प्रभाकर का ‘नियोग’ और शालिकनाथ का अदृष्ट ये निकटवर्ती शब्द हैं। चोदना वाक्य अर्थात् वाक्य जिसमें यज्ञ करने का आदेश है कत्र्ता में एक प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। यह प्रवृत्ति कत्र्ता को यत्नशील करती है। इसको नियोग कहते हैं। नियोग नियोज्य अर्थात् कर्ता में एक योग्यता उत्पन्न करता है जो कर्म की समाप्ति से लेकर फल की प्राप्ति तक रहती है। यही शक्ति ‘अपूर्व’ है। ‘अपूर्व’ इसलिये कहा कि यज्ञ से पूर्व यह न थी। यज्ञ करने से उत्पन्न हुई। फल के पश्चात् न रहेगी।१
यह अपूर्व चार प्रकार के माने गये हैं—
(१) फल-अपूर्व, (२) समुदाय-अपूर्व, (३) उत्पत्ति-अपूर्व, (४) अङ्ग-अपूर्व।
फल-अपूर्व वह मुख्य अपूर्व है जो अन्तिम फल की प्राप्ति कराता है।
समुदाय-अपूर्व समुदाय युक्त यज्ञों के हर एक समुदाय का अपना अलग अपूर्व है।
उत्पत्ति-अपूर्व उस समुदाय के हर एक यज्ञ का अपना अपूर्व है।
अङ्ग-अपूर्व हर उस छोटी क्रिया का अपूर्व है जो यज्ञ का अंग है।
कुछ यज्ञ कई यज्ञों के समुदाय नहीं हैं। उनके करने से फल अपूर्व उत्पन्न हो जाता है।
कुछ यज्ञ कई समुदायों को मिलाकर होते हैं। जैसे दर्शपौर्ण मास। इसके दो समुदाय हैं एक दर्श या अमावस्या को होने वाला। दूसरा पूॢणमा को। यह दोनों समुदाय अलग-अलग अपूर्व बनाते हैं जिनको समुदाय-अपूर्व कहते हैं।
इन समुदायों में से हर एक में तीन-तीन अवान्तर यज्ञ हैं जिनमें से हर एक उत्पत्ति-अपूर्व बनाता है।
इन यागों में कई छोटे-छोटे कृत्य हैं उनका अपूर्व अलग बनता है इसे अंग-अपूर्व कहते हैं।
पिछले यह तीनों अपूर्व मिलकर फल-अपूर्व बनाते हैं।
अब प्रश्न यह है कि चोदना-वाक्य का कौन-सा पद या शब्द अपूर्व का द्योतक है। जैमिनि आचार्य का मत है कि वाक्य का हर एक पद अलग-अलग भिन्न-भिन्न अपूर्व नहीं बतलाता। क्रिया पद जो विधिलिङ् है जैसे ‘यजेत’ वह अकेला भी अपूर्व नहीं बता सकता। वस्तुत: क्रियापद अन्य पदों से मिलकर उनकी सहायता से अपूर्व का द्योतक होता है।१
कर्म दो प्रकार के हैं एक प्रधान कर्म, दूसरे गौण कर्म। जो कर्म अपूर्व फल के लिये किये जाते हैं और जिनका फल दृष्ट नहीं है, अर्थात् जिस क्रियाओं द्वारा कोई चीज न बनाई जाती, न संस्कृत की जाती है, वे प्रधान कर्म हैं। जैसे यजति=यज्ञ करता है, जुहोति=होम करता है, ददाति=दान करता है। इनमें जो द्रव्य काम में लाये जाते हैं जैसे पुरोडाश, घृत या स्वर्ण आदि ये मुख्य नहीं, गौण हैं। मुख्य तो यज्ञ है। जो द्रव्य होम में काम आता है उसे गुण कहते हैं। और जिन कर्मों द्वारा वह द्रव्य बनाये या शोधे जाते हैं वे गौण कर्म कहलाते हैं। जैसे ‘व्रीहीन् वहन्ति’=धान कूटती है, ‘तन्दुलान् पिनष्टि’=चावल पीसती है, ‘यूपं तक्षति’=खम्भे को बनाता है, यहां कूटना, पीसना, बनाना गौण कर्म हैं।
मुख्य कर्मों में धान, चावल आदि द्रव्य पदार्थ गौण होते हैं। प्रधान नहीं। कर्म यजति, जुहोति आदि प्रधान हैं। गौण कर्मों में द्रव्य प्रधान है कर्म अप्रधान या गौण हैं। गौण कर्मों का फल दृष्ट होता है। अर्थात् सब जानते हैं कि धान कूटने से चावल निकलता है या चावल पीसने से आटा निकल आता है। गौण कर्मों का अपूर्व नहीं होता। प्रधान कर्मों का अपूर्व बनता है। जैसे यजति, जुहोति, ददाति, अपूर्व फल की दृष्टि से प्रधान कर्म ही मुख्य यज्ञ हैं। गौण कर्म तो लौकिक व्यापार मात्र हैं जो यज्ञ के साधनों को जुटाने के लिए हैंं।१
स्रुवा को मांजना, आग को ठीक करना, परिधियों को ठीक करना, पुरोडाश को अग्नि पर रखना यह गौण कर्म हैं। सक्तून् जुहोति=सत्तुओं से होम करता है। यह प्रधान कर्म है।२ स्तोत्र मंत्रों का गान करना और शस्त्र मंत्रों का पाठ करना यह प्रधान कर्म है।३
मन्त्रों और ब्राह्मणों दोनों को परिभाषिक रूप से वेद कहा है अर्थात् याज्ञिकों की परिभाषा में जहां मन्त्रों का अभिप्राय हो वहां भी और जहां ब्राह्मणों का अभिप्राय हो वहां भी ‘वेद’ शब्द का ही प्रयोग हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण वचनों में मन्त्रों को विनियोग के साथ कथित किया है। गंगा की लहर भी गंगा ही है क्योंकि नहर वह प्रदेश है जहां गंगा-जल कृषि के काम में आता है।
मन्त्र और ब्राह्मण के ऐसे पूरे लक्षण नहीं किये गये जिन में अति व्याप्ति, अव्याप्ति दोष न हों। केवल मोटी पहचान दे दीगई है, जैसे—
मन्त्रों की पहचान—
(१) जिनके अन्त में ‘असि’ हो, जैसे—‘मेधोऽसि।’
(२) जिनके अन्त में ‘त्वा’ ही, जैसे, ‘इषे त्वा।’ (यजुर्वेद १.१)
(३) आशीर्वाद, जैसे, ‘आयुर्दा असि’ (तै०सं० १.१.६)
(४) स्तुति, जैसे, ‘अग्निर्मूर्धा’ (तै०सं० ४.४.४.१)
(५) संख्या, जैसे, ‘एको मम’ (श०ब्रा० १.५.५.१२)
(६) प्रलाप, जैसे, ‘अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले दुलेरिव।’
(७) शोक मेें रोना, जैसे ‘अम्बे, अम्बिके।’ (यजु० २३.१८)
(८) प्रैष, (किसी काम के करने की आज्ञा), जैसे, ‘अग्नीदग्नीन्....’ (तै०सं० ६.३.२)।
(९) अन्वेषण, जैसे ‘कोसि कतमोसि’ (यजु० ७.२९)
(१०) प्रश्न—जैसे ‘पृच्छामि त्वा’ (यजु० २३.६१)
(११) आख्यान, जैसे ‘इयं वेदि’ (यजु० २३.६२)
(१२) अनुषङ्ग (बीच में प्रसङ्ग से दूर की कोई बात कह देना) (जुमला मुअतरिजा ) जैसे ‘अच्छिद्रेण पवित्रेण’ (तै०सं० १.१.५.१)
(१३) प्रयोग, जैसे ‘त्रैस्वर्यं, चातु:स्वर्यं’
(१४) सामथ्र्य अर्थात् अभिधाशक्ति।
ये उदाहरण प्रायिक हैं, यह बातें ब्राह्मण वाक्यों में भी मिलती हैं।
ब्राह्मण वाक्यों की भी मोटी पहचान दी है—
(१) जहां ‘इति’ बहुत आवे। (इति करण बहुलम्)
(२) ‘इति आह’ ऐसा कहते हैं। जहां आवे। (इत्याह उप-निबद्धम्)।
(३) हेतु: ‘जैसे शूर्पेण जुहोति, तेनह्यन्नं क्रियते।’ (श०ब्रा० २.५.२.२३)।
(४) आख्यायिका स्वरूप—
(५) निर्वचन, ‘जैसे तद् दध्नो दधित्वम्।’ (तै०सं० २.५.३.४)।
(६) निन्दा, ‘जैसे उपवीता वा एतस्य अग्नय:।’
(७) प्रशंसा, ‘जैसे वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता’ (तै०सं० २.१.१)।
(८) संशय, ‘जैसे होतव्यं, गार्हपत्ये न होतव्यम्।’
(९) विधि, ‘जैसे यजमान सम्मिता उदुम्बरी भवति।’
(१०) परकृति:, ‘जैसे माषानैव मह्यं पचति।’ (दूसरे का किया काम)।
(११) पुराकल्प (प्राचीन इतिहास), जैसे ‘उल्मुकैर्ह स्म पूर्वे समाजग्मु:।’
(१२) व्यवधारण कल्पना (्रह्यह्यह्वद्वश्चह्लद्बशठ्ठ शद्घ ञ्जह्म्ड्डठ्ठह्यश्चशह्यद्बह्लद्बशठ्ठ) जैसे ‘यावतोऽश्वान् प्रतिगृöीयात्।’
ये लक्षण सब जगह ठीक नहीं बैठते। अत: सर्वसाधारण के लिये यह नियम बता दिया कि जिनको आचार्यों ने ‘मन्त्र’ कहा वह मंत्र हैं, शेष ब्राह्मण।
‘ऊहा’, ‘प्रवर’, ‘नामधेय’ मन्त्र नहीं हैं क्योंकि आचार्यों ने इनको मन्त्र नहीं कहा।
ऊहा कहते हैं मन्त्र में कुछ अवसरोचित परिवर्तन कर देना। जैसे मन्त्र में था ‘अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि।’ यहां हवि का देवता ‘अग्नि’ है। जब आहुति ‘सूय्र्य’ के लिये दी गई तो ‘अग्नये त्वा’ के स्थान में पढऩे वाले ने ‘सूय्र्याय त्वा’ ऐसा पाठ पढ़ दिया। यह ‘ऊह’ है।
‘प्रवर’ मन्त्र के साथ यजमान के गोत्र या पूर्वज का नाम जोड़ देते हैं। यह ‘प्रवर’ है।
जब यजमान या उसके पुत्र, पौत्र का नाम लिया जाय तो इसको ‘नामधेय’ कहते हैं। कुमारिल आचार्य का कहना है कि मन्त्रों का उतना ही भाग अमन्त्र है जिसमें ऊह, प्रवर या नामधेय का कथन है। शेष मन्त्र मन्त्र ही है।
अब ऋक्, यजु और साम के लक्षण दिये हैं—
(१) ऋक् या ऋचायें वे हैं जिनमें अर्थ के वश से पाद- व्यवस्था है।
(२) जो गाये जायें उनको साम कहते हैं। अर्थात् यदि कोई ऋचा सामगान की विधि से गाई जाय तो उस गान का नाम साम है। जिस ऋचा पर वह गान गाया जाता है उस साम की वह ऋचा ‘योनि’ कहलाती है।
(३) शेष मन्त्र यजु हैं।१
एक ऋत्विज् दूसरे ऋत्वि को सम्बोधन करने में जो शब्द बोलता है वह निगद कहलाते हैं। निगद को आचार्य ने ‘यजु’ की कोटि में ही लिया है। ‘यानि च यजूंषि उच्चैरुच्चार्यन्ते ते निगदा:। ......न च पर सम्बोधनार्थ यजुषामुपांशुत्वं साहायां वर्तते’ (देखो भाष्य सूत्र २.१.४२)। साधारणतया यजुओं को धीमी आवाज से बोला जाता है। परन्तु धीमी आवाज से दूसरा पुरुष सुन नहीं सकता। अत: सम्बोधनार्थ जो यजु बोले जाने हैं वे उच्च स्वर से बोले जाते हैं उनका नाम निगद है।
कभी-कभी एक वाक्य के अन्तर्गत ऐसे पद आ जाते हैं जो दूसरे वाक्य के अर्थों की पूॢत में सहायक होते हैं। उनको ‘अनुषङ्ग’ कहते हैं।१ ‘साकाङ्क्षस्य सन्निधौ परस्तात् पुरस्तात् वा परिपूर्ण समर्थ: श्रूयमाणो वाक्य शेषो भवति।’ (भा०सू० २.१.४८)
अनुषङ्ग के प्रयोग का नियम यह है ‘आनन्तर्यं सम्बन्धि पद व्यवायो वा’। अर्थात् या तो आनन्तर्य हो अर्थात् बीच में कोई शब्द न आवे या यदि व्यवधान हो तो सम्बन्धी हो। सम्बन्धि-व्यवधान का अर्थ यह है कि ‘पूर्व’ और ‘पर’ में एक दूसरे की आकांक्षा होनी चाहिये। इसका एक उदाहरण दिया है—‘चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्य त्वा सविता पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो: सूय्र्यस्य रश्मिभि:।’ यहां ‘अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो: सूय्र्यस्य रश्मिभि:’ यह पद अनुषङ्ग है। क्योंकि पहले तीन वाक्य अपने अर्थ की पूॢत के लिये इस की आकांक्षा करते हैं।